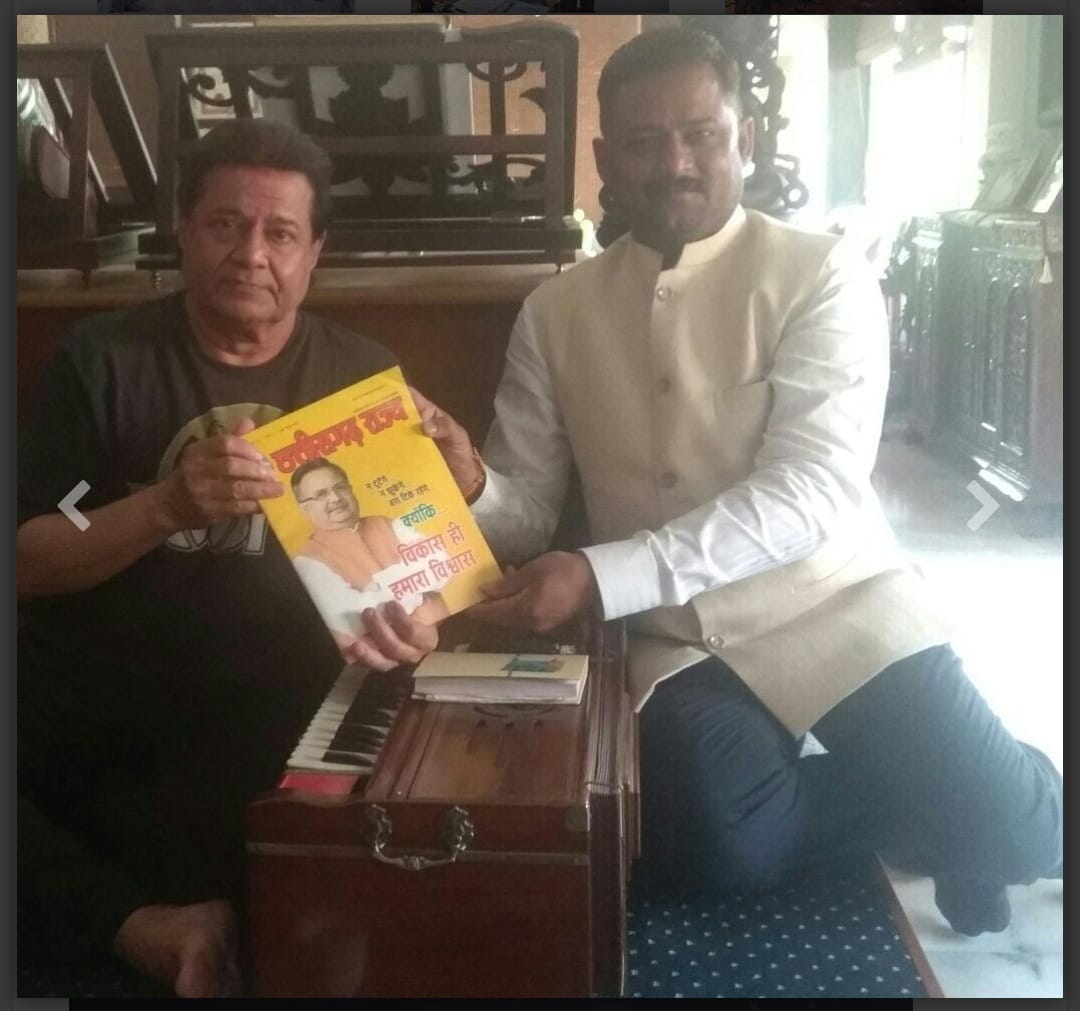मुफ्त सुविधाओं और चुनावी रेवडिय़ों की राजनीति पर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़े एक गंभीर प्रश्न को फिर से केंद्र में ला दिया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिस स्पष्टता और कठोरता के साथ राज्यों को आईना दिखाया है, वह केवल कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि आर्थिक और नैतिक चेतावनी भी है.
न्यायालय ने पूछा है कि क्या करदाताओं के धन का उपयोग अस्पताल, विद्यालय और सडक़ों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नहीं होना चाहिए. जब अनेक राज्य राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं, तब चुनाव के समय स्कूटी, कपड़े, मुफ्त बिजली और अन्य वस्तुएं बांटना किस प्रकार की वित्तीय समझदारी को दर्शाता है. यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की दिशा से जुड़ा हुआ है.
लोकतंत्र में कल्याणकारी योजनाएं आवश्यक हैं. निर्धनों, वंचितों और कमजोर वर्गों को सहायता देना राज्य का दायित्व है. किंतु सहायता और तुष्टीकरण के बीच एक महीन रेखा होती है. जब बिना किसी अंतर के सक्षम और असक्षम सभी को समान रूप से मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं, तो यह सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि वोट की राजनीति प्रतीत होती है. सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि जो लोग भुगतान करने में समर्थ हैं, उन्हें भी मुफ्त लाभ देना अंतत: उन गरीब बच्चों के अधिकारों पर आघात है जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती चिकित्सा की आवश्यकता है.
सबसे गंभीर प्रश्न कार्य संस्कृति पर पडऩे वाले प्रभाव का है. यदि नागरिकों को यह संदेश दिया जाए कि श्रम और उत्पादन के बिना भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं निरंतर मुफ्त मिलती रहेंगी, तो परिश्रम की प्रेरणा क्षीण हो सकती है. किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी कार्य संस्कृति, उद्यमिता और उत्पादकता पर निर्भर करती है. मुफ्त की आदत यदि मानसिकता बन जाए, तो यह आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर करती है.
चुनाव से ठीक पहले की जाने वाली अचानक घोषणाएं भी लोकतांत्रिक नैतिकता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं. जब दरें और बजट पूर्व निर्धारित होते हैं, तब अचानक खजाना खोल देना क्या जनहित का निर्णय है या मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास. तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम से जुड़े मामले में मुफ्त बिजली के कारण बढ़ते वित्तीय बोझ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी नीतियों का भार अंतत: सार्वजनिक उपक्रमों और करदाताओं पर ही पड़ता है.
राज्य सरकारों को यह समझना होगा कि अल्पकालिक लोकप्रियता और दीर्घकालिक विकास में से किसी एक का चयन करना पड़ता है. सुदृढ़ बुनियादी ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार सृजन ही स्थायी समृद्धि का मार्ग हैं. यदि संसाधन सीमित हैं, तो प्राथमिकताएं भी स्पष्ट होनी चाहिए.
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन और उत्तरदायित्व की पुकार के रूप में देखा जाना चाहिए. लोकतंत्र में मतदाता भी उतने ही उत्तरदायी हैं जितनी सरकारें. उन्हें यह विचार करना होगा कि क्या तात्कालिक लाभ दीर्घकालिक विकास की कीमत पर स्वीकार्य है.
समय आ गया है कि राजनीति लोकलुभावन वादों से ऊपर उठकर जवाबदेह शासन की ओर अग्रसर हो. कुल मिलाकर मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर परिश्रम, उत्पादकता और न्यायसंगत कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाना ही राष्ट्रहित में है. जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों और चिंता का राज्य और केंद्र सरकारों ने संज्ञान लेना चाहिए.